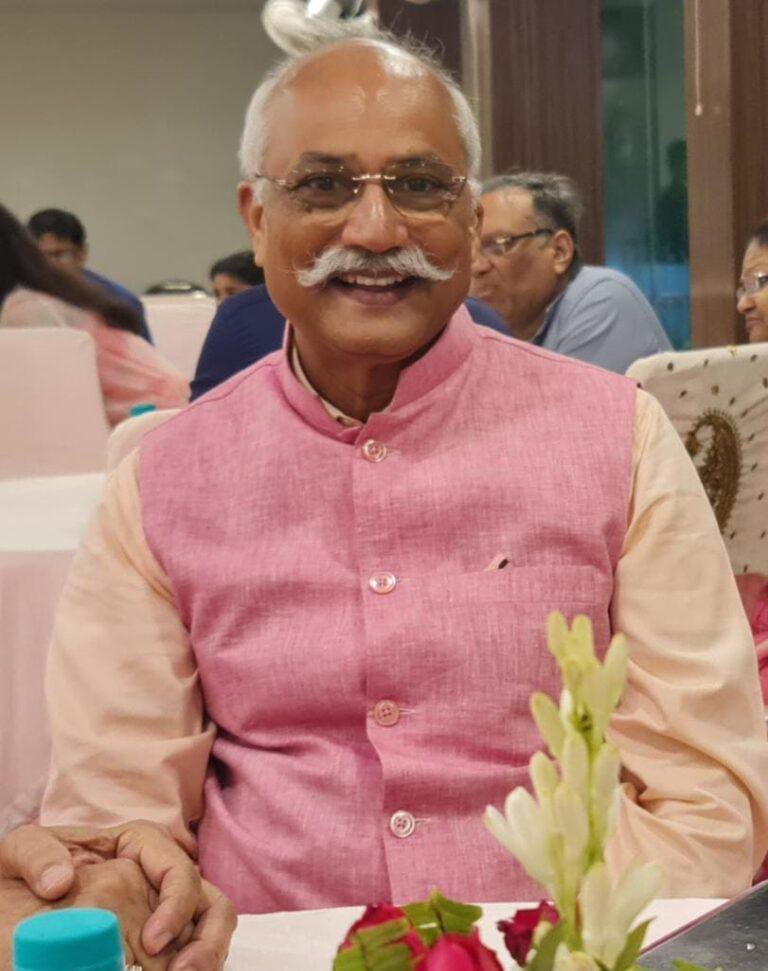
दैनिक इंडिया न्यूज़,लखनऊ।सफलता को यदि केवल पद, प्रतिष्ठा या भौतिक उपलब्धियों के संकुचित धरातल पर परिभाषित किया जाए, तो यह मानव जीवन की सबसे गंभीर वैचारिक भ्रांति होगी। सफलता वस्तुतः किसी लक्ष्य-प्राप्ति का नाम नहीं, बल्कि उस आंतरिक चेतन अवस्था का बोध है, जहाँ मनुष्य स्वयं को सीमाओं, भय और आत्मसंशय से मुक्त कर लेता है। यह वह स्थिति है, जहाँ व्यक्ति अपनी अंतर्निहित संभावनाओं को केवल पहचानता ही नहीं, बल्कि उन्हें धारण करने की पात्रता भी अर्जित करता है।
राष्ट्रीय सनातन महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा कि समाज में असफलता का मूल कारण परिश्रम का अभाव नहीं, बल्कि पात्रता और चेतना का असंतुलन है। अधिकांश लोग कर्म तो करते हैं, परंतु वह कर्म उनके अंतःकरण की परिपक्वता से आगे निकल जाता है। बाह्य श्रम तीव्र होता है, किंतु आंतरिक विकास मंद। यही कारण है कि प्रयत्न करते-करते मनुष्य थक जाता है और अंततः यह मान बैठता है कि सफलता उसके भाग्य में नहीं लिखी।
वस्तुतः मनुष्य जब कर्मरत होता है, तब उसका मन पूर्णतः मुक्त नहीं होता। उसके भीतर एक सूक्ष्म किंतु निरंतर सक्रिय भय कार्य करता रहता है—असफल होने का भय, आलोचना का भय, समाज की दृष्टि का भय। “यदि मैं आगे बढ़ गया और विफल हुआ तो लोग क्या कहेंगे?” यह प्रश्न व्यक्ति की ऊर्जा को भीतर ही भीतर क्षीण कर देता है। यह भय वास्तविक नहीं होता, किंतु इसका प्रभाव अत्यंत वास्तविक होता है। यही भय मनुष्य को उसकी सामर्थ्य की सीमा तक पहुँचने से बहुत पहले रोक देता है।
यह भी एक कटु यथार्थ है कि संसार आपके संघर्ष से अधिक आपके परिणामों को देखता है। समाज आपकी नीयत नहीं, आपकी उपलब्धि को स्मरण रखता है—और अधिकांश समय वह आपको स्मरण भी नहीं रखता। इस सत्य को स्वीकार कर लेना ही मानसिक स्वतंत्रता की प्रथम सीढ़ी है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि समाज की दृष्टि उसकी कल्पना जितनी सर्वव्यापी नहीं है, उसी दिन उसके भीतर का भय अपनी शक्ति खो देता है।
परंतु इससे भी गहन सत्य यह है कि हर परिश्रमी व्यक्ति को समान सफलता क्यों नहीं मिलती। यहाँ सनातन दर्शन एक मौलिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है—पात्रता का सिद्धांत। ईश्वर की व्यवस्था कर्म के साथ-साथ पात्रता को भी देखती है। जैसे बीज और भूमि का संबंध होता है—बीज चाहे जितना श्रेष्ठ हो, यदि भूमि उपयुक्त न हो, तो अंकुरण संभव नहीं। उसी प्रकार, सफलता भी उसी को प्राप्त होती है, जिसकी चेतना, संयम और संस्कार उस सफलता को धारण करने योग्य होते हैं।
यही कारण है कि अनेक बार हम देखते हैं—जो अत्यंत परिश्रमी होते हैं, वे पीछे रह जाते हैं; और कुछ लोग अपेक्षाकृत कम संघर्ष में आगे बढ़ जाते हैं। इससे उत्पन्न होती है कटुता। असफल व्यक्ति आगे बढ़ने वालों को देखकर ईर्ष्या, द्वेष और अविश्वास से भर जाता है। वह यह मानने लगता है कि संसार अन्यायी है या ईश्वर पक्षपाती। किंतु वास्तव में वह ईश्वर की उस योजना को नहीं देख पाता, जिसके अंतर्गत सफलता केवल पुरस्कार नहीं, उत्तरदायित्व भी होती है।
ईश्वर कभी भी उस मनुष्य को ऊँचाई नहीं देता, जो ऊँचाई को संभाल न सके। जिनके भीतर अहंकार प्रबल होता है, जिनका मन अस्थिर होता है, जिनकी चेतना संकीर्ण होती है—उन्हें ईश्वर प्रगति से रोक देता है, दंड देने के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए। और जिनका मन निर्मल, उद्देश्य व्यापक और भाव सेवा-प्रधान होता है, उन्हें सफलता स्वयं खोजती है।
सफलता तब तक स्थायी नहीं हो सकती, जब तक उसका संबंध केवल बुद्धि और गणना से हो। लक्ष्य यदि मात्र योजना का परिणाम बन जाए, तो वह शीघ्र ही बोझ में परिवर्तित हो जाता है। वास्तविक शक्ति तब जन्म लेती है, जब लक्ष्य भावना से जुड़ जाता है। जब अंतःकरण यह कह उठता है—“इसके बिना मेरा जीवन अधूरा है”—तब मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं रह जाता, वह साधक बन जाता है।
दर्शन कहता है कि कर्म तब फलदायी होता है, जब वह साधना का स्वरूप ग्रहण कर ले। साधना का अर्थ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि ऐसा कर्म, जिसमें मनुष्य स्वयं को अर्पित कर दे। जब कर्म साधना बनता है, तब संघर्ष पीड़ा नहीं देता, और थकान भी अर्थपूर्ण प्रतीत होती है।
यहाँ एक सूक्ष्म किंतु निर्णायक अंतर समझना आवश्यक है—स्वप्न मन को लुभाता है, किंतु लक्ष्य मनुष्य को अनुशासित करता है। स्वप्न सुविधा चाहता है, लक्ष्य त्याग की माँग करता है। जो व्यक्ति असुविधा को स्वीकार नहीं कर पाता, वह ऊँचाइयों की यात्रा नहीं कर सकता। शिखर उन्हीं के लिए सुरक्षित होते हैं, जो असफलता को अपमान नहीं, बल्कि शिक्षण प्रक्रिया का अनिवार्य चरण मानते हैं।
सफलता का वास्तविक विस्तार तब प्रारंभ होता है, जब लक्ष्य का केंद्र केवल “मैं” न रहकर “हम” बन जाता है। जब मनुष्य अपने कर्म को परिवार, समाज, राष्ट्र और मानवता से जोड़ देता है, तब उसके भीतर एक उच्चतर चेतना का उदय होता है। यह चेतना केवल प्रगति की नहीं, बल्कि संतुलन, करुणा और विवेक की भी होती है।
धन जीवन का आवश्यक साधन है, किंतु उसे ही सफलता का पर्याय मान लेना दृष्टि की संकीर्णता है। धन साधन है, साध्य नहीं। वास्तविक सफलता वह है, जहाँ मन स्थिर हो, संबंध जीवंत हों और आत्मा निरंतर परिष्कृत होती रहे। जिन समाजों में विघटन और तनाव दिखाई देता है, वहाँ समस्या साधनों की नहीं, बल्कि साझा उद्देश्य और भावनात्मक संवाद के अभाव की होती है।
अतः प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं से यह प्रश्न अवश्य पूछना चाहिए—क्या मैं केवल जीवन का निर्वाह कर रहा हूँ, या जीवन को अर्थ प्रदान कर रहा हूँ? जिस दिन यह प्रश्न मनुष्य को भीतर से विचलित कर देता है, उसी दिन उसकी चेतना जाग्रत हो जाती है। और जाग्रत चेतना को न भय रोक सकता है, न आलोचना, न परिस्थितियाँ।
सफलता उसी क्षण आरंभ हो जाती है, जब मनुष्य स्वयं से समझौता करना त्याग देता है। उसके पश्चात साधारण प्रयास भी असाधारण परिणाम देने लगते हैं, क्योंकि तब कर्म के पीछे केवल इच्छा नहीं, पात्रता से युक्त चेतना खड़ी होती है।
