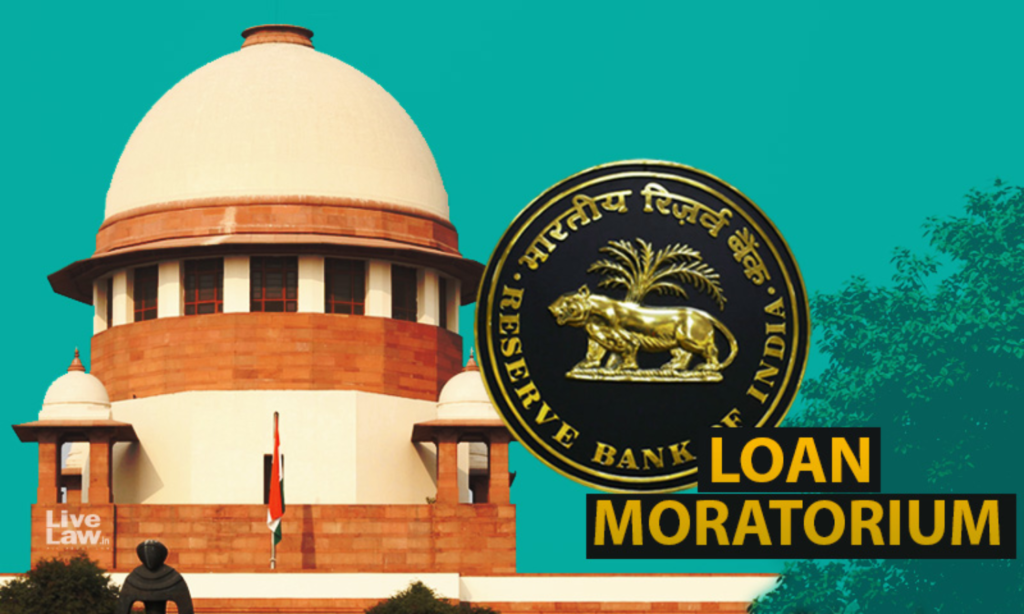
“जब कानून कहता है ‘गोपनीयता’, तो रिकवरी एजेंट क्यों बजा रहे हैं ढिंढोरा?”
हरिंद्र सिंह,दैनिक इंडिया न्यूज़ नई दिल्ली।लोन लेना आज की आधुनिक ज़िंदगी का अनिवार्य हिस्सा बन चुका है। चाहे घर खरीदना हो, गाड़ी लेनी हो, बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाना हो या अचानक कोई आर्थिक आपातकाल सामने आ जाए—हर स्थिति में लोग बैंक और वित्तीय संस्थानों की ओर रुख करते हैं। बैंक भी आसान किस्तों पर लोन उपलब्ध कराते हैं, जिससे लोगों को लगता है कि उनकी परेशानियां कम हो जाएंगी। लेकिन असली समस्या तब खड़ी होती है जब लोन लेने वाला व्यक्ति समय पर ईएमआई नहीं चुका पाता। तीन बार तक लगातार ईएमआई बाउंस होने का मतलब होता है कि बैंक उस खाते को ‘नॉन-परफॉर्मिंग एसेट’ (NPA) घोषित कर देगा।
यहीं से शुरू होता है ग्राहक की असली परीक्षा। बैंक या एनबीएफसी के रिकवरी एजेंट घर पहुंचते हैं और कई बार ऐसा व्यवहार करते हैं जो न केवल कर्जदार बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए अपमानजनक और कष्टदायी होता है। कानून साफ कहता है कि लोन लेने वाले की जानकारी केवल उसी व्यक्ति तक सीमित रहेगी, यहां तक कि पत्नी या घरवालों को भी यह जानकारी साझा करने का प्रावधान नहीं है। इसके बावजूद अकसर देखा जाता है कि रिकवरी एजेंट मोहल्ले के लोगों को बता देते हैं कि अमुक व्यक्ति लोन नहीं चुका रहा है। यह न केवल आरबीआई की गाइडलाइन्स का उल्लंघन है बल्कि कर्जदार की निजता के अधिकार पर भी चोट है।
उदाहरण के तौर पर लखनऊ के एक व्यक्ति ने पांच लाख रुपये का पर्सनल लोन लिया था। अचानक नौकरी चली जाने की वजह से लगातार तीन महीने ईएमआई बाउंस हो गई। बैंक ने उसे डिफॉल्टर घोषित कर दिया और रिकवरी एजेंट उसके घर पहुंचा। एजेंट ने न केवल उसकी पत्नी को बताया कि लोन बकाया है, बल्कि पड़ोसियों के सामने भी जोर-जोर से चिल्लाकर कहा कि यह व्यक्ति पैसे नहीं चुका रहा। इसके बाद मोहल्ले में उसकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल गई और पत्नी मानसिक रूप से परेशान हो गई। जबकि कानूनी तौर पर यह पूरी तरह गलत था।
आरबीआई ने रिकवरी एजेंटों के लिए सख्त गाइडलाइन बनाई हैं। एजेंट केवल सुबह आठ बजे से शाम सात बजे तक ही ग्राहक से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें हमेशा अधिकृत पहचान पत्र और बैंक का लिखित पत्र दिखाना जरूरी है। एजेंटों को आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से प्रशिक्षण और प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य है। बैंक भी अपने एजेंटों की हरकतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि कोई एजेंट बदतमीजी करता है, तो बैंक पर जवाबदेही बनती है और ग्राहक को अधिकार है कि वह बैंकिंग लोकपाल या आरबीआई में शिकायत दर्ज कराए।
कानूनी प्रक्रिया भी स्पष्ट है। यदि 90 दिनों तक ईएमआई नहीं चुकाई जाती तो लोन NPA घोषित हो जाता है। इसके बाद बैंक तेजी से कदम उठाते हैं। अगर छह महीने यानी 180 दिन तक भी भुगतान नहीं होता, तो बैंक अदालत का सहारा ले सकता है। चेक बाउंस की स्थिति में Negotiable Instruments Act, Section 138 के तहत आपराधिक केस भी दर्ज हो सकता है। यदि लोन सुरक्षित है, जैसे होम लोन, तो SARFAESI Act, 2002 लागू होता है, जिसके तहत बैंक बिना कोर्ट गए संपत्ति ज़ब्त कर सकता है और नीलामी करके पैसा वसूल सकता है।
कानपुर की एक महिला का उदाहरण लें। उसने पंद्रह लाख रुपये का होम लोन लिया था। महामारी के दौरान उसकी आय बंद हो गई और छह महीने तक ईएमआई नहीं चुकाई जा सकी। बैंक ने संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी। मामला अदालत पहुंचा तो कोर्ट ने कहा कि बैंक को पहले समुचित नोटिस देना होगा और ग्राहक को वन टाइम सेटलमेंट का विकल्प देना चाहिए। अदालत ने महिला को राहत दी। यह घटना बताती है कि अदालतें कई बार उपभोक्ता के हित में हस्तक्षेप करती हैं ताकि बैंक मनमानी न कर सकें।
अब सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की बात करें तो उन्होंने समय-समय पर बैंकों और एजेंटों की मनमानी पर रोक लगाई है। 2008 के ICICI Bank vs Shanti Devi Sharma मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिकवरी एजेंटों द्वारा दबाव बनाने की रणनीति अनुचित है और यह कई बार व्यक्ति को आत्महत्या तक के लिए मजबूर कर सकती है। अदालत ने कहा कि बैंक को कानूनी और नैतिक दायरे में रहकर ही वसूली करनी चाहिए। इसी तरह State Bank of Travancore vs Mathew K.C. (2018) में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि SARFAESI एक्ट के तहत जब वैधानिक उपाय मौजूद हैं, तो हाई कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे स्पष्ट होता है कि अदालतें चाहती हैं कि बैंक अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करें, लेकिन साथ ही कर्जदार को भी नियमों का पालन करना पड़ेगा।
हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि केवल पैसे की वसूली के लिए आपराधिक कानून का इस्तेमाल करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि ऋण विवादों का निपटारा सिविल अदालत में होना चाहिए, न कि पुलिस केस बनाकर। यह फैसला खासतौर पर उन मामलों में महत्वपूर्ण है, जहां बैंक या प्राइवेट एजेंसियां कर्जदारों को डराने के लिए एफआईआर दर्ज करा देती हैं। एक और उदाहरण में सुप्रीम कोर्ट ने हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर न मिलने पर होमबायर्स को राहत दी और कहा कि जब तक मकान नहीं दिया जाता, तब तक उन्हें ईएमआई नहीं चुकानी पड़ेगी। यह फैसला दर्शाता है कि अदालतें केवल बैंक के हितों को नहीं देखतीं बल्कि उपभोक्ताओं के अधिकारों को भी प्राथमिकता देती हैं।
ग्राहकों के पास भी कई अधिकार हैं। यदि कोई एजेंट बिना पहचान पत्र या बैंक के लिखित अधिकृत पत्र के घर आता है तो ग्राहक उसे रोक सकता है। यदि एजेंट गाली-गलौज करता है या पड़ोसियों को बताकर बदनाम करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धाराओं में शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। बैंकिंग लोकपाल और आरबीआई जैसी संस्थाएं भी उपभोक्ता को राहत देने के लिए बनी हैं। जरूरत इस बात की है कि ग्राहक अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों और हर नोटिस या कॉल का लिखित रिकॉर्ड रखें।
हालांकि मौजूदा कानून में एक बड़ी खामी यह है कि अगर तीन महीने तक ईएमआई बाउंस हो जाती है तो बैंक पूरा पैसा एक साथ मांग सकते हैं। यह व्यावहारिक नहीं है कि कोई व्यक्ति अचानक पूरी राशि चुका सके। इस कारण इसे कई लोग उपभोक्ता विरोधी और अव्यावहारिक प्रावधान मानते हैं। यही वजह है कि समय-समय पर विशेषज्ञ और उपभोक्ता संगठन इस कानून में बदलाव की मांग करते रहे हैं।
कुल मिलाकर, ईएमआई बाउंस और रिकवरी प्रक्रिया सिर्फ वित्तीय नहीं बल्कि सामाजिक और मानसिक समस्या भी बन चुकी है। बैंक और एजेंट जहां सख्ती दिखाते हैं, वहीं उपभोक्ता अक्सर अपमान और दबाव में आ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और आरबीआई के दिशा-निर्देश उपभोक्ताओं को सुरक्षा देने का प्रयास करते हैं, लेकिन जब तक लोग अपने अधिकारों को नहीं समझेंगे और कानून का सहारा नहीं लेंगे, तब तक यह समस्या बनी रहेगी। बैंक और उपभोक्ता के बीच संतुलन तभी बनेगा जब वसूली प्रक्रिया पारदर्शी और मानवीय होगी और कानून का पालन दोनों पक्ष करेंगे।
